भारत के प्रधान मंत्री और उनका कार्यकाल | Prime Ministers of India and their tenure in hindi
भारत के प्रधानमंत्री, Prime Ministers of india, भारत के अब तक के सारे Prime Ministers, Prime Ministers के काम, कौन-कौन थे भारत देश के Prime Ministers, prime ministers of india essay in hindi.
जब हम स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमारे द्वारा भारत के Prime Ministers द्वारा निभाई गई भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए। आज इस लेख में, हम भारत के Prime Ministers की सूची को कवर करते हुए यह जानने वाले है की आखिर कैसा रहा था उनका कार्यकाल।
भारत का Prime Ministers भारत सरकार की कार्यपालिका के नेता होता है। साथ ही प्रधान मंत्री भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी होते हैं। प्रधान मंत्री भारत की संसद के दो सदनों लोकसभा और राज्य सभा (राज्यों की परिषद) में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन उन्हें उस राजनीतिक दल का सदस्य होना चाहिए, जिनका लोकसभा में बहुमत हो।
तो आइए अब हम भारत के उन लोगों के बारे में जाते है, जिन्होंने भारत के Prime Ministers के रूप में कालानुक्रमिक क्रम में कार्य किया।
Table of Contents
भारत के अब तक बने Prime Ministers
जवाहर लाल नेहरू (पहली बार)
- पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तब वह फूलपुर से सांसद थे।
- स्वतंत्रता के बाद, 15 अगस्त 1947 को, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और प्रथम नेहरू मंत्रालय बनाने के लिए पंद्रह मंत्रियों को चुना और इसे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा नियुक्त किया गया।
- उनका पहला कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अप्रैल 1952 तक था।
जवाहर लाल नेहरू (दूसरी बार)
नेहरू का दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से लेकर 17 अप्रैल 1957 तक था।
जवाहर लाल नेहरू (तीसरी बार)
तीसरा नेहरू मंत्रालय 17 अप्रैल 1957 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1957 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद बनाया गया था। इस बार उनका कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से लेकर 2 अप्रैल 1962 तक था।
जवाहर लाल नेहरू (चौथी बार)
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साल 1962 के आम चुनाव में जीत के बाद 2 अप्रैल 1962 को चौथे नेहरू मंत्रालय का गठन किया गया था। नेहरू कुल 16 साल, 286 दिन तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे थे।
- उनका कुल कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक था।
गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक प्रधान मंत्री – पहली बार)
- गुलजारीलाल नंदा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, जो श्रम मुद्दों में विशेषज्ञता रखते थे।
- वह साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू और साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधान मंत्री बने थे।
- वह साबरकांठा से सांसद थे।
- सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए।
- उन्हें साल 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
- उनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 09 जून 1964 तक था।
- और उनका दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक था
लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri)
- वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता थे।
- वह साल 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए।
- साल 1947 में स्वतंत्रता के बाद, वह भारत सरकार में शामिल हो गए और प्रधान मंत्री नेहरू के प्रधानों में से एक बन गए।
- इसके बाद उन्होंने साल (1951-56) तक भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में काम किया, और फिर उन्होंने गृह मंत्रालय सहित कई अन्य कार्यों को भी संभाला।
- उन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया।
- तब “जय जवान जय किसान” (सैनिक की जय हो, किसान की जय हो) का उनका नारा युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ।
- उनका कार्यकाल 09 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था।
इंदिरा गांधी (पहली बार)
- वह भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधान मंत्री थीं।
- इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं।
- वह दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधान मंत्री थीं।
- उन्हें “द आयरन लेडी ऑफ इंडिया” के रूप में सराहा गया, और यह एक ऐसा उपनाम था, जो उनकी अडिग राजनीति और नेतृत्व शैली से पूरी तरह जुड़ गया।
- वह पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में पाकिस्तान के साथ युद्ध में गई, जिसके परिणामस्वरूप इस युद्ध में भारत जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- अलगाववादी प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए और क्रांति के आह्वान के जवाब में, गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति स्थापित की, जहां बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था और इसके साथ प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया।
- उनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक था।
इंदिरा गांधी (दूसरी बार)
इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक था।
इंदिरा गांधी (तीसरी बार)
- इंदिरा गांधी का तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक था।
- इस अवधि के दौरान, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अलगाववादी प्रवृत्तियों का हवाला देते हुए और क्रांति के आह्वान के जवाब में, गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल की स्थिति की स्थापना की।
मोरारजी देसाई (Morarji Desai)
- वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत के चौथे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार का नेतृत्व किया।
- देसाई भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- वह भारतीय राजनीति के इतिहास में 84 वर्ष की आयु में प्रधान मंत्री का पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे।
- उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था।
चरण सिंह (Charan Singh)
- उन्होंने भारत के 5वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- इतिहासकार और देश के लोग समान रूप से उन्हें अक्सर ‘भारत के किसानों के चैंपियन’ के रूप में संदर्भित करते हैं।
- उनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक है।
इंदिरा गांधी (चौथी बार)
- साल 1980 में, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बाद सत्ता में लौटीं।
- गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश देने के बाद, 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी।
- उनका तीसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था।
राजीव गांधी (Rajiv Gandhi)
- वह एक भारतीय राजनेता थे, जिन्होंने भारत के 6वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने 1984 में अपनी मां, प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, 40 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के भारतीय प्रधान मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया।
- प्रधान मंत्री के रूप में गांधी की पहली कार्रवाई जनवरी 1985 में दलबदल विरोधी कानून पारित कर रही थी।
- चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी।
- उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 01 दिसंबर 1989 तक था।
वी.पी. सिंह (V.P. Singh)
- वह 1989 से 1990 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे।
- साल 1969 में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए।
- 1988 में, उन्होंने जनता पार्टी के विभिन्न गुटों को मिलाकर जनता दल पार्टी का गठन किया। फिर 1989 के चुनावों में, भाजपा के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई और सिंह भारत के 7वें प्रधान मंत्री बने।
- प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भारत की पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया।
- उनका कार्यकाल 01 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था।
चंद्र शेखर (Chandra Shekhar)
- उन्होंने 10 नवंबर 1990 और 21 जून 1991 के बीच भारत के आठवें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने चुनावों में देरी के लिए एक स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहरी समर्थन के साथ जनता दल के एक अलग गुट की अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया।
- साल 1991 में भारतीय आर्थिक संकट और राजीव गांधी की हत्या ने उनकी सरकार को संकट में डाल दिया।
- वह पहले भारतीय प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने कभी भी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था।
पी.वी. नरशिमा राव (P.V. Narshima Rao)
- वह एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन की देखरेख करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रशासन का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घरेलू घटनाएं भी देखी गईं।
- उन्हें अक्सर “भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक” कहा जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक परिवर्तन शुरू करने के लिए डॉ मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया था।
- उन्होंने राजीव गांधी की सरकार की समाजवादी नीतियों को उलटते हुए लाइसेंस राज को खत्म करने में तेजी लाई।
- राव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विनाश भी देखा गया।
- उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था।
अटल बिहारी वाजपेयी (पहली बार)
- वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य थे।
- उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में तीन कार्यकालों की सेवा की, पहली बार 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए।
- उनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था।
एच.डी. देवेगौड़ा (H.D. Deve Gowda)
- वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधान मंत्री थे, और वे जनता दल (संयुक्त मोर्चा) सरकार का नेतृत्व कर रहे थे।
- साल 1996 के आम चुनावों में, किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं जीतीं। जब संयुक्त मोर्चा, क्षेत्रीय दलों के गठबंधन ने कांग्रेस के समर्थन से केंद्र सरकार का गठन किया, तब देवेगौड़ा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, और वे भारत के 11वें प्रधान मंत्री बने।
आई.के. गुजराल (I.K. Gujral)
- उन्होंने जनता दल (संयुक्त मोर्चा) सरकार का नेतृत्व करते हुए अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के 12वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- 1976 में, गुजराल ने सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। साल 1996 में, वह देवेगौड़ा मंत्रालय में विदेश मंत्री बने। वह ‘गुजराल सिद्धांत’ के लिए जाने जाते हैं।
- प्रधान मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष से भी कम समय तक चला।
अटल बिहारी वाजपेयी (दूसरी बार)
- एनडीए सरकार के तहत अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक था।
- प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, भारत ने 1998 में पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण किया। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार करने की मांग की, प्रधान मंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए बस से लाहौर की यात्रा की।
- साल 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद, उन्होंने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ सगाई के माध्यम से संबंधों को बहाल करने की मांग की, उन्हें आगरा में एक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आमंत्रित किया।
- उनका दूसरा कार्यकाल केवल 13 महीने तक चला।
अटल बिहारी वाजपेयी (तीसरी बार)
- एनडीए सरकार के तहत अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक था।
- वह पहले भारतीय प्रधान मंत्री थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, जिन्होंने कार्यालय में पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
डॉ मनमोहन सिंह (पहली बार)
- यह एक भारतीय अर्थशास्त्री, अकादमिक और राजनेता हैं, जिन्होंने भारत के 13वें प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक था।
- उनके पहले मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई प्रमुख कानूनों और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया।
- साल 2008 में, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
डॉ मनमोहन सिंह (दूसरी बार)
यूपीए (UPA) सरकार के तहत मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक था।
नरेंद्र मोदी (पहली बार)
- नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक था।
- उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए (NDA) सरकार का नेतृत्व किया, जो भारत की पहली गैर-कांग्रेसी एकल-दल बहुमत वाली सरकार थी।
- उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के विवादास्पद विमुद्रीकरण की शुरुआत की।
- इसके अलावा मोदी ने एक हाई-प्रोफाइल स्वच्छता अभियान भी शुरू किया था, और पर्यावरण और श्रम कानूनों में भी कई सुधार लाए थे।
- मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पांच साल पूरे करने वाले दूसरे गैर-कांग्रेसी पीएम बने।
नरेंद्र मोदी (दूसरी बार)
- पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 से अब तक का है।
- इसके साथ ही वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाहर पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दो बार जीतने वाले पहले प्रधान मंत्री बने हैं।
FAQ (Frequently Asked Questions)
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत के पहले प्रधानमंत्री “पंडित जवाहरलाल नेहरू” थे।
भारत के सबसे पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने?
भारत के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री “मोरारजी देसाई” थे।
भारत के किन Prime ministers की हत्या की गयी थी?
भारत के अब तक दो प्रधानमंत्री “इंद्रा गाँधी” और “राजीव गाँधी” की हत्या की जा चुकी है।
आशा करता हूं कि आज आपलोंगों को कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो हमारे बाकी के आर्टिकल्स को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ऱोज कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, और इस articleको अपने दोस्तों और जान पहचान वालो के साथ ज़रूर share करे जिन्हें इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।
Also read –
सुभाष चन्द्र बोस का जीवन परिचय
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय


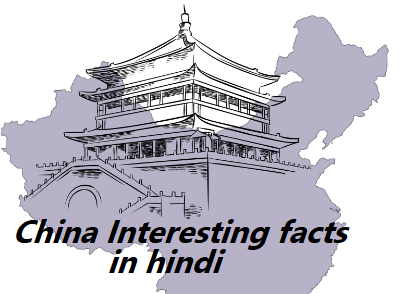




I was reading through some of your articles on this website and I believe this site is real informative ! Keep on putting up.
Metal reclaiming facility Ferrous metal reprocessing Iron scrap shearing
Ferrous material market outlook, Iron recycling and repurposing center, Metal salvage and recycling
You are so interesting! I do not think I’ve read a single
thing like this before. So great to discover someone with some unique thoughts on this
issue. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the
internet, someone with a little originality!
My site … vpn special
Link exchange is nothing else except it is simply placing the
other person’s blog link on your page at suitable
place and other person will also do similar for you.
Visit my web page – vpn coupon code 2024
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.